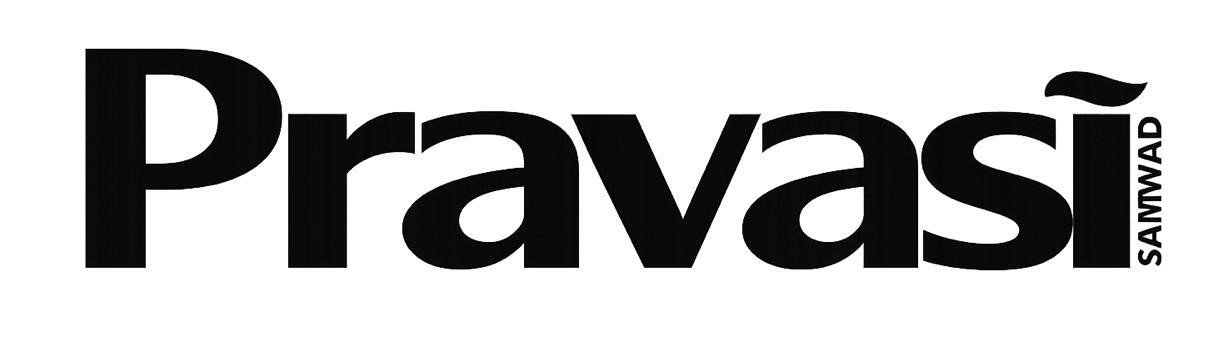सुदामा पांडेय धूमिल को पढ़ती हूँ तो जाने क्यों मुझे मंटो याद आते हैं .. नशे को तोड़ती हैं जैसे मंटो की कहानियाँ, वैसी ही कड़वाहट भरी गोली है धूमिल की कविताएँ …
सच का कसैलापन वैसा होगा जैसा सच होगा, दिखावे के मीठे आवरण धूमिल की अभिव्यक्ति पर नहीं चढ़ते। धूमिल सच की बोतल खोलने से घबराये ही नहीं , चाहे उस सच में संडास की या खोले हुए जूतों से आती पैरों की बदबू हो … वैसे ही सामने रख दिया है उन्होंने तथाकथित बुद्धिजीवियों के सामने, की ढँक लो अपने आभिजात्य या बौद्धिकता की रूमाल से अपनी नाक, अपनी दोगली नज़र वालीआँखें मींचे निकल लो !
रिश्तों का, बुद्धिजीवियों का, गाँव का या वो पेट की आग का सच हो, धूमिल वो ज्वालामुखी थे जिनसे सच का लावा निकलता था … अपनी कविताओं में पुरुषार्थ का थकना – हारना, विचलित होना , मरना सब बड़ी निष्ठुरता से उन्होंने चित्रित किया गया है, पर उसनिष्ठुरता के नेपथ्य में आम लोगों की लाचारी से भरी खामोश चीख सी लगातार गूंजती रहती है।
उनकी तुलना के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जब वे , निराशा, असंतोष , मोहभंग और बुद्धिजीवियों की अवसरवादिता को व्यक्त करते हैं । रोटी बेलने , खाने और खेलने की बात हो या ज़िंदा रहने के लिए पालतू होना ज़रूरी है , ज़ाहिर करती उनकी निराशा , आप जब भी किसी बेक़सूर आदमी का हलफ़नामा पढ़ते हैं , धूमिल के अंतस के चीत्कार से रु-ब-रु होते हैं।

उनकी कविता , “कुछ सूचनाएँ “में वे कहते हैं – सूरज कितना मजबूर है की हर चीज़ पर एक सा चमकता है ..
या फिर ,
“ हिजड़ों ने भाषण दिए लिंग – बोध पर
वेश्याओं ने कविता पढ़ी आत्म-शोध पर
प्रेम में असफल छात्राएँ अध्यापिका बन गयी हैं …
निराशा का अंधकार में उनके अंदर की कसक नूर बन कर चमकती है कैसे , ये देखिए –
“ जो भी मुझमें हो कर गुज़रा रीत गया
पता नहीं कितना अंधकार था मुझमें
मैं सारी उम्र चमकने की कोशिश में बीत गया …”
या फिर अपनी कविता “ गाँव” में वे लिखते हैं –
“ जीवित है वह जो बूढ़ा है या अधेड़ है
और हरा है – हरा यहाँ पर सिर्फ़ पेड़ है …” जिस तरह जवान नस्लों की आकांक्षाओं, जुनून, कुछ कर दिखाने के जोश की मृत्युगाथा अपनी इन पंक्तियों में वो दर्शाते हैं , वो बेमिसाल है ।
धूमिल की “सच्ची बात “का हथौड़ा समाज के सीने पर बेधड़क , एकदम सीधे पड़ता है जब वे कहते हैं –
“… वैसे हम समझते हैं कि सच्चाई
हमें अक्सर अपराध की सीमा पर
छोड़ आती है …”
और कौन उनके इस कहे हुए का मुरीद ना होगा –
“कितना भद्दा मज़ाक़ है
की हमारे चेहरों पर आँख के ठीक नीचे नाक है “ !!
धूमिल आज़ादी के पहले और बाद का ज़ख़्म खाया दिलो-जिगर रखते थे , जीवन मूल्यों और सामाजिक संरचना , अवसरवादिता औरज़िंदगी से जूझते मन – प्राण की एकदम नंगी तस्वीर प्रस्तुत करते रहे ,अपने इतने अल्प-काल के जीवन में। थोड़ा और जीते तो कहीं कुछ अधमरी लाशों में लड़ने का उत्साह जगाते, सच की आग से उन तमाम रास्तों को और रोशन करते जिस पर दर्द और डर से लोग चलते ही नहीं। धूमिल की लेखनी युगों तक धूमिल नहीं हो सकती … उनकी सच उगलती ज्वालामुखी रूपी कविताएँ कभी सुषुप्त नहीं हो सकतीं!
हमारी नयी नस्लों को धूमिल की समझ होनी चाहिए , जिस सुंदर सामाजिक परिदृश्य की कल्पना उन्होंने तब की थी , वो आज भी बहुत सामयिक है। जाने क्यों यहीं दुष्यंत कुमार का लहजा तुरत याद आता मुझे शायद इसलिए भी की दुष्यंत कुमार और धूमिल के दर्द और उसकी इंतहा कई मायनों में एक हैं , बस एक ज़रा अदायगी का फ़र्क़ है ..
“ये शफ़क़ शाम हो रही है अब
और हर गाम हो रही है अब
जिस तबाही से लोग बचते थे
वो सर-ए – आम हो रही है अब .. “