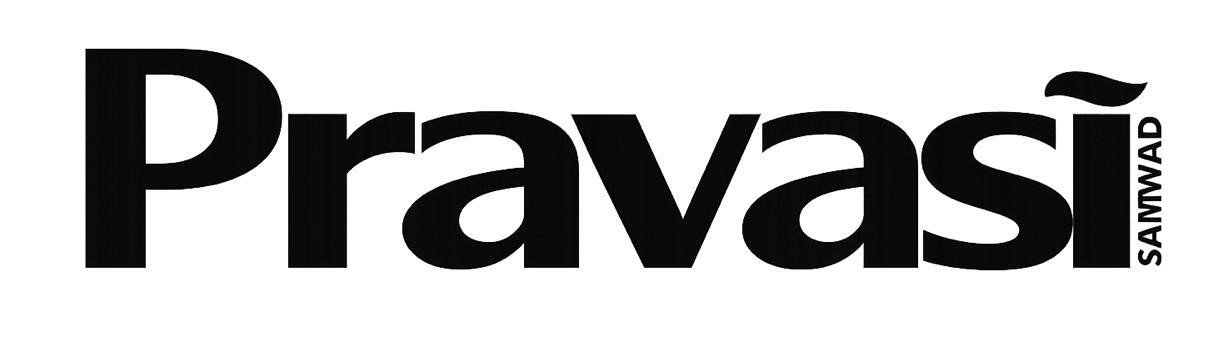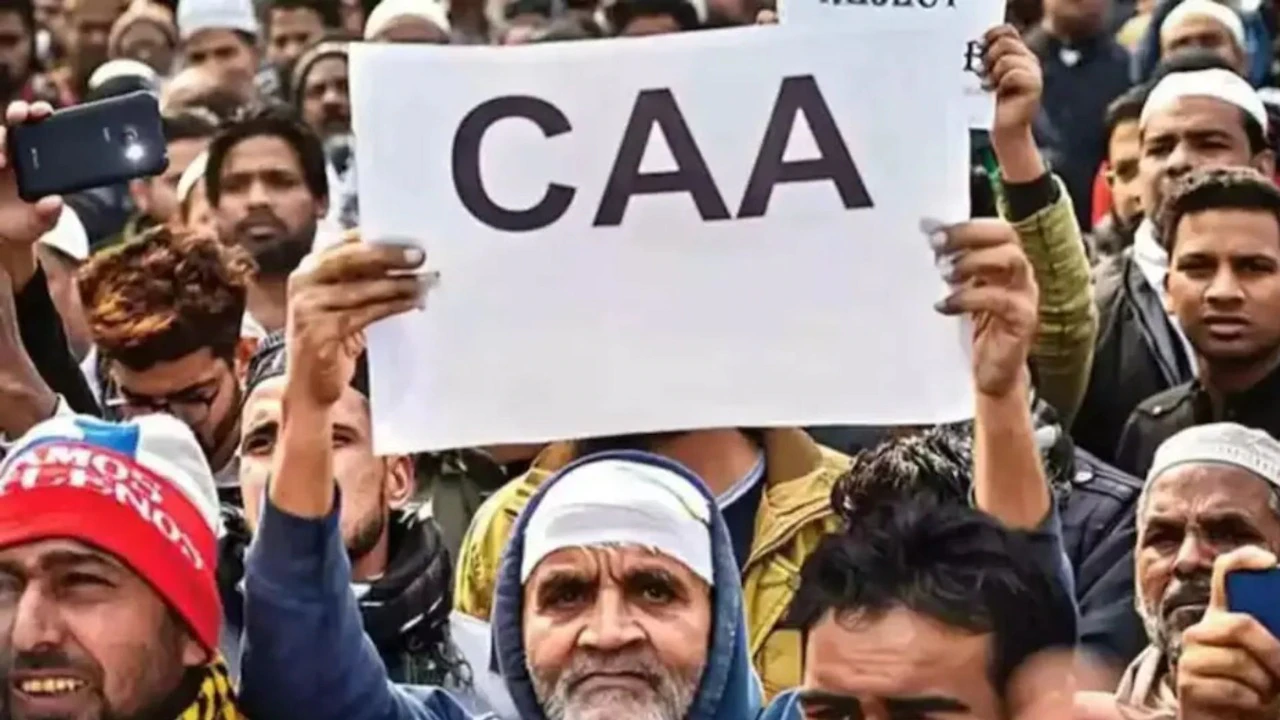आनंदवर्धन ओझा
बिहारी भारत के किसी कोने में रहे,वह अपनी प्रवृत्ति से विवश रहता है. गर्मियों में उसे चाहिए आम-लीची-बेल, हर मौसम में सत्तू, सुबह के नाश्ते में जलेबी-कचौड़ी-घुघनी और शाम के वक़्त भंजा, गाय-बकरी की तरह दिन-भर जुगाली करने को चाहिए मगही पान और सुगंधित तम्बाकू. छठ व्रत के समय ठेकुए खजूर के लिए उसका जी मचलता है और होली के मौसम में गुझिया पेडुकिया के लिए उसकी आत्मा ऐंठने लगती है और, किसी भी दशा में प्रतिदिन रीति-नीति-राजनीति तथा साहित्य पर बतकुच्चन के लिए उसे चाहिए मित्रों संघतियों की एक टोली, अपने बहुत करीब.
अजीब जीव होता है बिहारी, मेहनतकश, श्रमजीवी और हठी भी. किसी भी काम के लिए तत्पर, यह कहता हुआ “होइबे नहीं करेगा? अरे, होगा कइसे नहीं?” और बिहार रत्न कविवर दिनकर लिख भी तो गए हैं-
“खम ठोंक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पांव उखड,
मानव जब जोर लगता है,
पत्थर पानी बन जाता है.”
दिनकरजी की इस ललकार की अनसुनी कर देने वाला भला बिहारी कैसे हो सकता है? उस पर तुर्रा ये कि बिहारी अगर ब्राह्मण हुआ तो उसका विलक्षण मिष्टान्न-प्रेम तो जग जाहिर है ही. कहा गया है ना, ‘विप्रम्मधुरं प्रियं!’ इसी कथन का उल्लेख करते हुए एक बार किसी ने कहा था- ‘पंडित जी तो ऐसे मिष्टान्न-प्रेमी होते हैं कि गुड़ का एक टुकड़ा कहीं डाल दीजिए, पंडित जी वहीं चिपके मिलेंगे.’ मुझे लगता है, भले आदमी नेबहुत गलत नहीं कहा था.
पिछले साल अक्टूबर में, छठ पूजा के बाद,आस लगी रही कि बिहार से कोई-न-कोई आएगा, छठ के ठेकुए लाएगा.पांच-दस मुझे भी प्रसाद केरूप में दे जाएगा. सो,प्रतीक्षारत रहा और पलटते पन्नोंकी तरह दिन बीतते रहे, बिहार से कोई भलामानुस आया ही नहीं और ठेकुए की लालसा में जीमचलता रहा, आत्मा ऐंठती ही रही.
आख़िरश, एक दिन बिहारी का ब्रह्मतेज जागा, हठधर्मी, श्रमजीवी और स्वाबलंबी जो ठहरा. श्रीमती जी विद्यालय गयी थीं. पूरे घर में मेरा साम्राज्य था. मैंने गुड़ की भेली उठाई.भई, पुणे का गुड़ था-पत्थरदिल था, तोड़े न टूटता था. मैंने उसे नरमदिल बनाने केलिए धीमी आंच पर पानी में डालकर चढ़ा दिया. बगल के कमरे में टी.वी.ऑन था.
महत्त्व का एक समाचार कानों पड़ा तो मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुआ और समाचार सुनाने लगा. अचानक गुड का ख़याल आया. किचेन में दौड़कर पहुंचा.पत्थरदिल गुड़ तो मोम-सा पिघलकर लेई बन गया था और खौल रहा था. मैंने शीघ्रता से बर्नर बुझाया और आटे में उसे मिलाकर हाथ जला- जला कर गूंथने लगा. खोजकर पटनहिया सांचा निकाला और उस पर परिश्रमपूर्वक आटे की छोटी-छोटी गोलियों को ठेकुए की आकृति मेंढालने लगा. जैसे-जैसे गुंथा हुआ आटा ठंढा होता जा रहा था, वैसे-वैसे वह पथराता जा रहा था.
अब तो सांचे पर दबने में भी उसे आपत्ति थी. मेरे हठी और श्रमजीवी मनने हठ न छोड़ा. बिहारी के स्वाभिमानी मन में दो ही वाक्य गूंज रहे थे- ‘तू हैबिहारी, तो कर परिश्रम, हार गया, तो बिहारी कैसा?’
लीजिये हुजूर, घंटों के श्रम का प्रतिफल हुआ कि अब शक्लो-सूरत से ठेकुए तैयार थे, बस, उन्हें रिफाइंड में डूब उतरा कर और थोड़ी देर नर्तन कर कड़ाही से बाहर आना भर था. श्रीमती जी के विद्यालय से लौट आने के पहले ही यह कृत्य भी पूरा हुआ. ठेकुए तो देखते ही बनते थे- तले हुए लाल लाल,सोधे-कुरकुरे ठेकुए लेकिन अभी गर्म थे, मुंह में डाल लेने का रिस्क कौन लेता? सुविज्ञ बिहारी तो हरगिज़ नहीं.
ठेकुए के शीतल होने की प्रतीक्षा हो ही रही थी कि श्रीमतीजी आ पहुंचीं. घर में पांव रखते ही चहकीं- “क्या बना है घर में? बड़ी सुगंध आ रही है.क्या बनाया है ‘मेड’ ने?”
मैंने गौरव से भरकर कहा- ‘ठेकुए बनाये हैं मैंने, खस्ते और कुरकुरे,टुह टुह लाल.’
श्रीमती जी को सहसा विश्वास नहीं हुआ,विस्फारित नेत्रों से मुझे घूरते हुए बोलीं- ‘आपने?’
श्रीमती जी को सहसा विश्वास नहीं हुआ,विस्फारित नेत्रों से मुझे घूरते हुए बोलीं- ‘आपने?’
मेरा जी तो अगराया हुआ था, छाती ठोंकते हुए मैंने कहा- ‘हां भई, मैंने.’
दो-तीन घंटों बाद ठेकुए जी ठंडे पड़े, एक मैंने, एक श्रीमती जी ने मुश्किल से खाए, मेरा मन रखने को श्रीमती जी ने नरमदिली से कहा- ‘मोयन नहींडाला क्या? ठेकुआ थोड़ा कड़ा हो गया है.’
मैं भला क्या कहता ? ‘मोयन’ शब्द से पहली बार मुलाकात जो हुई थी.
दूसरे दिन जब ठेकुए बिलकुल ठंडे पड़ गए. मैं बड़ी हसरत से उनके पास गया.थोड़ी देर तक निहारता रहा उन्हें. दिखने में तो वे बहुत सुदर्शन थे, आकर्षित करते थे अपनी ओर, किन्तु पुणे के गुड की तरह पत्थर दिल हो गये थे रात भर में. मन मारकर रह गया,दांत से उसका एक टुकड़ा भी काटलेना असंभव था. मेरा सारा उत्साह भी ठंडा पड़ने लगा.
सप्ताह-भर में श्रीमती जी ने ऐलानिया घोषणा कर दी कि ये ठेकुए असाध्य, असंभव खाद्य-सामग्री हैं. उन्होंने स्टील का एकबड़ा कटोरदान ठेकुओंसे भरकर कबर्ड के किसी एकांत में झोंक दिया और शेष ठेकुओंको एक पॉलिथीन में भरकर काम वाली बाई को देदिया, इस हिदायत के साथ कि लोढ़े से तोड़-कूचकर अपने बच्चों को खाने को दे.बाई तो खुश हुई,लेकिन मिष्टान-प्रेमी बिहारी का मन मुरझा गया. वह सोचता ही रहा कि जिन ठेकुओं के लिए स्वयंपाकी बना, उनकी रक्षा वह कैसे करे?
लेकिन एक डेढ़ महीना बीत गया, ठेकुए तो मन से उतर ही गए थे, यादों की गलियोंमें कहीं खो भी गए.
व्यंग्य वह जनवरी का महीना था. उस दिन भी घर परमेरा ही आधिपत्य था.जैसे चूहा किसी खाद्य-सामग्री के लिए घुरियाता है, ठीक वैसे ही सुबहके जलपान के बाद किसी मीठी सामग्री की तलाश में भटकता हुआ मैं कबर्ड में रखे कटोरदान तक जा पहुंचा. बहुत दिनों के बाद उन्हें देखकर मनमें हर्ष की लहर दौड़ गई. मैंने एक ठेकुआ उठाया और बांयीं दाढ़ से तोड़ने की कोशिश की.वज्र ठेकुआ काहे को टूटता? मैंने बायीं दाढ़ से भरपूरजोर लगाया और तभी दायीं दाढ़ में कनपटी के पास नगाड़े बज उठे- ‘कड़-कड़-कड़’, दिन में तारे देखने का सुख तो मिला,लेकिन असहनीय पीड़ाभी हुई. दायें कल्ले पर हाथ रखकर अपनी चौकी पर धम्म से जा बैठा.
दोपहर में जब श्रीमतीजी आयीं, तब तक तो दायें जबड़े पर सूजन आ गयी थी.उन्होंने मेरी हालत देखी तो दांतों तले अपनी ऊंगली दबा ली,फिर गुस्से से बोलीं- ‘इन नामुराद ठेकुओं पर मुंह मारने की क्या जरूरत थी? मैं तो इन्हें फेंकने ही वाली थी.’ मैं अपने मिष्टान्न प्रेम पर शर्मिंदा होने केसिवा और कर भी क्या सकता था.
दूसरे दिन दंत-चिकित्सक के पास गया और महीने भर की दवाएं लेक रलौट आया. दवाओं के सेवन से तात्कालिक आराम तो हुआ, लेकिन मेरा मुंह तो कड़कड़डूमा की अदालत बन गया है.
मित्रो, वह एक अकेला ठेकुआ मुझे कम-से-कम एक हजार रुपये का तो पड़ ही गया और जबड़े का दर्द अपनी जगह कायम है. आज भी कुछ खाता हूं तो दायां जबड़ा ‘कड़कड़ कड़कड़’ बोलता है. लगता है, लोहे के चने चबा रहा हूं. लेकिन बिहारी तो बिहारी ठहरा, ज़िद्दी, श्रमजीवी और संघर्षशील. उसका पान और ठेकुआ प्रेम आज भी यथावत बना हुआ है. लेकिन, सोचता हूं,क्या ज़रूरी था मेरी दाढ़ तोड़ के जाना उसका? जानेअब कब मिलेगा पथराए ठेकुओं की जगह मीठा, मुलायम, खस्ता और कुरकुरा ठेकुआ.